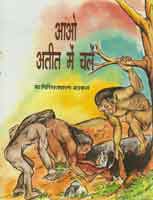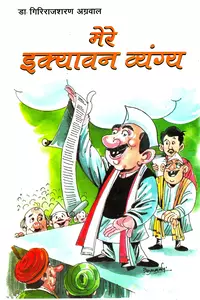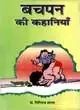|
बाल एवं युवा साहित्य >> आओ अतीत में चलें आओ अतीत में चलेंगिरिराजशरण अग्रवाल
|
11 पाठक हैं |
||||||
किशोर आयु के बालकों के लिए प्रस्तुत है आदि मानव पर आधारित पुस्तक..
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आदि से आधुनिक तक
किशोर अवस्था के पाठक और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-सामग्री कैसी हो ? आज
के वैज्ञानिक युग में यह प्रश्न और भी जटिल हो गया है। इसका कारण यह है कि
प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य के विचार स्थिर, दृष्टिकोण लगभग अपरिवर्तनीय और
सोचने-समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता दृढ़ हो चुकी होती है। इस
अवस्था में आदमी एक विशेष ढाँचे में ढल चुका होता है, जबकि किशोर अवस्था
निर्माण की प्रक्रिया से गुजर कर उस रूप-स्वरूप की तरह बढ़ रही होती है,
जो निकट भविष्य में उसे ग्रहण करना होता है। इस आयु-वर्ग के बच्चों के
सामने रखने पर यह प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि उनके लिए
इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य तथा ऐसे अन्य विषयों से संबंधित
पाठ्य-सामग्री कैसी हो, वह किस शैली में लिखी जाए, जिससे किशोरों का
मनोरंजन भी हो और उनके चिंतन में व्यापकता, स्वभाव में तर्कप्रियता तथा
दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता उत्पन्न हो। ऐसी पाठ्य-सामग्री उनके लिए रोचक
भी होगी और भ्रांतियों को दूर करने वाली भी। किंतु खेद की बात है कि
वर्तमान में किशोरों के लिए जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश इस
कसौटी पर पूरी नहीं उतरतीं। परिणामतः किशोर अवस्था की लोचदार बुद्धि किसी
बने-बनाए ढाँचे में ढलकर एक ही तरह के मनुष्यों को ढालती रहती है। यह
परंपरागत शिक्षा न तो उन्हें कोई नया रास्ता ही सुझाती है और न उन
भ्रांतियों को ही दूर कर पाती है, जो शताब्दियों की उलट-फेर के कारण
सामाजिक जीवन में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं।
इतिहास ही को लें। किशोर अवस्था के बालकों को जिस तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है या वे स्वयं पढ़ते हैं, उनमें राजाओं, महाराजाओं और सामंतों-सम्राटों के संबंध में दी गई ऊपरी जानकारी से अधिक कुछ नहीं होता। इस विवरण से किशोर अवस्था के बालक केवल इतना ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं कि किस सम्राट् ने अपने जीवनकाल में कितने युद्ध लड़े, किस युद्ध में उसे विजय मिली, किसको पराजय मिली, किसके पास कितनी सैनिक शक्ति थी, किसकी सेना किस तरह के हथियार प्रयोग करती थी, किसने कौन-कौन से युद्ध लड़कर किन-किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, उसके शासन में सीमाएँ कहाँ से कहाँ तक थीं? इससे आगे इन पुस्तकों में अगर कुछ बताया जाता है तो केवल इतना कि इन सम्राटों में किसने अपने शासनकाल में क्या-क्या नियम बनाए, सामाजिक व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किए, उसके शासन में जनता सुखी थी या दुखी, उसने कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे भवन बनाए, कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया, उसके युग में साहित्य की और अन्य कलाओं की कितनी प्रगति हुई ? इसके आगे कुछ नहीं...
इन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किशोर अवस्था के पाठकों को मात्र यह विश्वास दिलाता है कि सामाजिक जीवन चलाने, बनाने और बिगाड़ने की समस्त निर्णायक शक्ति राजा-महाराजाओं के हाथ में रही है। इनमें से कुछ तो आदर्श एवं ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में स्थापित भी हो चुके हैं। यह पुस्तक उन्हें उनके उच्च एवं सम्मानित स्थान से नीचे नहीं उतारती, केवल यह बताती है कि मानव-विकास की यात्रा में ये नायक, ये आदर्श पुरुष, ये सम्राट किस तरह उत्पन्न हुए, वे कौन-सी स्थितियाँ थीं, जिनके कारण कुछ लोग निर्बल हो गए तो कुछ सबल, कुछ साधन-संपन्न हो गए तो कुछ साधनविहीन, कुछ स्वामी बन गए तो कुछ दास। वस्तुतः यह पुस्तक इतिहास के घटनाक्रम को सम्राटों-शासकों की धुरी पर नहीं घुमाती, यह मानव-समाज के प्राकृतिक प्रवाह में उनकी उत्पत्ति के वैज्ञानिक कारणों को प्रस्तुत करती है। यह राजाओं का लेखा-जोखा नहीं है। यह मानव की उस लंबी यात्रा का दर्पण है, जो इतिहासपूर्व में गुफाओं से चलकर वर्तमान स्थिति को दिखाता है। पुस्तक की विशेषता यह है कि इसे एक रोचक कहानी के रूप में लिखा गया है। कथावाचक, जो अपने हुलिए और वाणी से स्वयं भी एक रोचक व्यक्ति है, बच्चों के सामने एक दिलचस्प कहानी के रूप में उस यात्रा का वर्णन करता है, जो आदिमानव ने अपने उदय के प्रारंभिक काल में गुफाओं के आवास से शुरू की थी। पुस्तक बताती है कि तब वह कैसा था, किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था, उसकी दिनचर्या क्या थी, आहार जुटाने के क्या साधन उसके पास थे, समूह के रूप में गुफाओं का जीवन व्यतीत करने वाले आदिमानव की आस्थाएँ कैसी थीं, वह किस प्रकार सोचता था, किस प्रकार अपनी सोच व्यक्त करता था ? यह किशोर आयु के बालकों के लिए ही नहीं, प्रौढ़ अवस्था के विद्यार्थियों एवं पाठकों के लिए भी अत्यंत रुचिकर है।
लेखक ने मानव-विकास के इतिहास का जिस तरह वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उससे उस पुस्तक का गुणात्मक महत्त्व और भी बढ़ जाता है।
विक्रम दा नाम का एक व्यक्ति शरद ऋतु में प्रतिदिन उस छोटे कस्बे में आता है, जो अभी नगर या महानगर नहीं बना है। बच्चों के सामने एक चौपाल में बैठकर वह उन्हें मानवजाति का इतिहास कहानी के रूप में सुनाता है। ये बच्चे नहीं जानते थे कि अब चौबीस-पच्चीस लाख वर्ष पहले वे कैसे थे और अपना विकास करते-करते वे किस प्रकार उस मोड़ पर आए, जहाँ वे आज दिखाई दे रहे हैं।
विक्रम दा उन्हें बताते हैं, गुफाओं के जीवन से निकलकर बस्तियाँ बसाने तक मानव ने किस प्रकार संघर्ष किया? गोत्र कैसे निर्मित हुए और फिर गोत्रों से समुदायों की स्थापना कैसे हुई? ये समुदाय आगे चलकर कबीलों में कैसे परिवर्तित हुए। कबीलों का सरदार कैसे बना ? गाँवों में मुखियाओं की उत्पत्ति क्यों हुई? ये सरदार और मुखिया किस प्रकार शक्तिशाली होते गए? किस प्रकार इन्होंने अन्य सरदारों के क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार किया? किस प्रकार छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई? किस प्रकार छोटे राज्यों से बड़े राज्य अस्तित्व में आए? किस प्रकार ये राज्य एक देश के नाम से जाने गए? कई-कई देशों सी.सी. विश्लेषण रोचक भी है और ज्ञानवर्द्धक भी।
पुस्तक केवल यही बताती नहीं है कि आदमी का सामाजिक विकास कैसे हुआ, वह यह भी बताती है कि आदिमानव में धार्मिक आस्थाओं की उत्पत्ति किस कारण हुई, अंधविश्वास किस कारण जड़ पकड़ते गए, धर्मों की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उन्होंने मानव-जीवन के विकास में क्या योग दिया तथा संभ्रांत एवं सत्ताधारी वर्गों ने धर्मों को अपने हित में प्रयोग कर उनसे कैसा और क्या लाभ उठाया? पुरोहितों और सामंतों के गठजोड़ ने मानव-समाज पर क्या प्रभाव डाला? यह सारा विवरण कथावाचक ने शायद जान-बूझकर धर्मो के आध्यात्मिक पहलू पर बहस नहीं की है। उसका कारण संभवतः यह है कि अलौकिक शक्तियों की वास्तविक पहचान अथवा परमेश्वर की सत्यता का ज्ञान इस पुस्तक की विषयवस्तु नहीं था। कथावाचक का विषय तो धार्मिक आस्थाओं की उत्पत्ति, उनका विकास तथा मानव-जीवन पर उनके प्रभाव को प्रदर्शित करना मात्र था। वही कथावाचक ने किया है। आदिमानव ने जिस रूप में आस्थाओं को ग्रहण किया, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। आदिमानव अपने विकास के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा था। इस संघर्ष में जो शक्तियाँ उसके ज्ञान की पकड़ तथा अधिकार की पहुँच से बाहर रहीं, वह उन्हें अपने विश्वासों और अपनी आस्थाओं के साथ जोड़ता गया। इन्हीं आस्थाओं और विश्वासों की नींव पर बाद में बड़े-बड़े धर्म खड़े हुए। धर्मगुरुओं तथा सूफी-संतों ने आगे चलकर आदिमानव की इस सोच की वास्तविकता का पता चलाया, उससे भ्रांतियों को अलग किया तथा जो सत्य उनके ज्ञान में आया, उसे धर्म में जोड़ दिया।
पुस्तक मानव जाति के इन्हीं पहलुओं से ही नहीं बल्कि कई अन्य पहलुओं से भी बहस करती है। यह बताती है कि मानव-समाज में पेशों के आधार पर जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई, कलाओं और शिल्पों का जन्म कैसे हुआ, साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, आदमी ने लिपि किस प्रकार सीखी, आदिमानव किस चीज पर लिखा करता था? पत्थर युग से धातु युग से आज परमाणु युग तक आदमी ने जो लंबी यात्रा की है, उसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में बहुत ही रोचक ढंग से हुआ है।
मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक किशोर अवस्था के बालकों की भ्रांतियाँ ही दूर नहीं करेगी, बल्कि परंपरागत शिक्षा के परिणामस्वरूप बने उनके चिंतन में भी गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।
मैं अपनी यह बात फिर जोर देकर कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक का सबसे बड़ा उद्देश्य आदमी की कथा को आदमी तक ही केंद्रित रखना है। उसे राजाओं, बादशाहों का बहीखाता न बनाकर तार्किक रूप से यह सिद्ध करना है कि मानव-समाज में विकास या परिवर्तन की जो मौलिक शक्तियाँ रही हैं, वे आदमी की विकसित, प्रभावित या परिवर्तित होती हुई सोच और उत्पादन के अदलते-बदलते साधनों से जुड़ी थीं। यह सही है कि आदिमानव के सामूहिक जीवन में कुछ व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक विकसित हुए तो कुछ कम, जैसे कि एक परिवार के चार बच्चों के बीच देखा जाता है। इस असमानता ने भी अधिक प्रबुद्ध और शक्तिशाली लोगों को अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों पर धाक जमाने की प्रेरणा दी होगी। बहरहाल, यह पुस्तक जिस रोचक एवं वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई है, उसके लिए लेखक निसंदेह प्रशंसा का पात्र है। इसे अधिक से अधिक हाथों में पहुँचना चाहिए, क्योंकि यह मानव-इतिहास को उसके सच्चे रूप में प्रस्तुत करती है।
इतिहास ही को लें। किशोर अवस्था के बालकों को जिस तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है या वे स्वयं पढ़ते हैं, उनमें राजाओं, महाराजाओं और सामंतों-सम्राटों के संबंध में दी गई ऊपरी जानकारी से अधिक कुछ नहीं होता। इस विवरण से किशोर अवस्था के बालक केवल इतना ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं कि किस सम्राट् ने अपने जीवनकाल में कितने युद्ध लड़े, किस युद्ध में उसे विजय मिली, किसको पराजय मिली, किसके पास कितनी सैनिक शक्ति थी, किसकी सेना किस तरह के हथियार प्रयोग करती थी, किसने कौन-कौन से युद्ध लड़कर किन-किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, उसके शासन में सीमाएँ कहाँ से कहाँ तक थीं? इससे आगे इन पुस्तकों में अगर कुछ बताया जाता है तो केवल इतना कि इन सम्राटों में किसने अपने शासनकाल में क्या-क्या नियम बनाए, सामाजिक व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किए, उसके शासन में जनता सुखी थी या दुखी, उसने कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे भवन बनाए, कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया, उसके युग में साहित्य की और अन्य कलाओं की कितनी प्रगति हुई ? इसके आगे कुछ नहीं...
इन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किशोर अवस्था के पाठकों को मात्र यह विश्वास दिलाता है कि सामाजिक जीवन चलाने, बनाने और बिगाड़ने की समस्त निर्णायक शक्ति राजा-महाराजाओं के हाथ में रही है। इनमें से कुछ तो आदर्श एवं ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में स्थापित भी हो चुके हैं। यह पुस्तक उन्हें उनके उच्च एवं सम्मानित स्थान से नीचे नहीं उतारती, केवल यह बताती है कि मानव-विकास की यात्रा में ये नायक, ये आदर्श पुरुष, ये सम्राट किस तरह उत्पन्न हुए, वे कौन-सी स्थितियाँ थीं, जिनके कारण कुछ लोग निर्बल हो गए तो कुछ सबल, कुछ साधन-संपन्न हो गए तो कुछ साधनविहीन, कुछ स्वामी बन गए तो कुछ दास। वस्तुतः यह पुस्तक इतिहास के घटनाक्रम को सम्राटों-शासकों की धुरी पर नहीं घुमाती, यह मानव-समाज के प्राकृतिक प्रवाह में उनकी उत्पत्ति के वैज्ञानिक कारणों को प्रस्तुत करती है। यह राजाओं का लेखा-जोखा नहीं है। यह मानव की उस लंबी यात्रा का दर्पण है, जो इतिहासपूर्व में गुफाओं से चलकर वर्तमान स्थिति को दिखाता है। पुस्तक की विशेषता यह है कि इसे एक रोचक कहानी के रूप में लिखा गया है। कथावाचक, जो अपने हुलिए और वाणी से स्वयं भी एक रोचक व्यक्ति है, बच्चों के सामने एक दिलचस्प कहानी के रूप में उस यात्रा का वर्णन करता है, जो आदिमानव ने अपने उदय के प्रारंभिक काल में गुफाओं के आवास से शुरू की थी। पुस्तक बताती है कि तब वह कैसा था, किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था, उसकी दिनचर्या क्या थी, आहार जुटाने के क्या साधन उसके पास थे, समूह के रूप में गुफाओं का जीवन व्यतीत करने वाले आदिमानव की आस्थाएँ कैसी थीं, वह किस प्रकार सोचता था, किस प्रकार अपनी सोच व्यक्त करता था ? यह किशोर आयु के बालकों के लिए ही नहीं, प्रौढ़ अवस्था के विद्यार्थियों एवं पाठकों के लिए भी अत्यंत रुचिकर है।
लेखक ने मानव-विकास के इतिहास का जिस तरह वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उससे उस पुस्तक का गुणात्मक महत्त्व और भी बढ़ जाता है।
विक्रम दा नाम का एक व्यक्ति शरद ऋतु में प्रतिदिन उस छोटे कस्बे में आता है, जो अभी नगर या महानगर नहीं बना है। बच्चों के सामने एक चौपाल में बैठकर वह उन्हें मानवजाति का इतिहास कहानी के रूप में सुनाता है। ये बच्चे नहीं जानते थे कि अब चौबीस-पच्चीस लाख वर्ष पहले वे कैसे थे और अपना विकास करते-करते वे किस प्रकार उस मोड़ पर आए, जहाँ वे आज दिखाई दे रहे हैं।
विक्रम दा उन्हें बताते हैं, गुफाओं के जीवन से निकलकर बस्तियाँ बसाने तक मानव ने किस प्रकार संघर्ष किया? गोत्र कैसे निर्मित हुए और फिर गोत्रों से समुदायों की स्थापना कैसे हुई? ये समुदाय आगे चलकर कबीलों में कैसे परिवर्तित हुए। कबीलों का सरदार कैसे बना ? गाँवों में मुखियाओं की उत्पत्ति क्यों हुई? ये सरदार और मुखिया किस प्रकार शक्तिशाली होते गए? किस प्रकार इन्होंने अन्य सरदारों के क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार किया? किस प्रकार छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई? किस प्रकार छोटे राज्यों से बड़े राज्य अस्तित्व में आए? किस प्रकार ये राज्य एक देश के नाम से जाने गए? कई-कई देशों सी.सी. विश्लेषण रोचक भी है और ज्ञानवर्द्धक भी।
पुस्तक केवल यही बताती नहीं है कि आदमी का सामाजिक विकास कैसे हुआ, वह यह भी बताती है कि आदिमानव में धार्मिक आस्थाओं की उत्पत्ति किस कारण हुई, अंधविश्वास किस कारण जड़ पकड़ते गए, धर्मों की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उन्होंने मानव-जीवन के विकास में क्या योग दिया तथा संभ्रांत एवं सत्ताधारी वर्गों ने धर्मों को अपने हित में प्रयोग कर उनसे कैसा और क्या लाभ उठाया? पुरोहितों और सामंतों के गठजोड़ ने मानव-समाज पर क्या प्रभाव डाला? यह सारा विवरण कथावाचक ने शायद जान-बूझकर धर्मो के आध्यात्मिक पहलू पर बहस नहीं की है। उसका कारण संभवतः यह है कि अलौकिक शक्तियों की वास्तविक पहचान अथवा परमेश्वर की सत्यता का ज्ञान इस पुस्तक की विषयवस्तु नहीं था। कथावाचक का विषय तो धार्मिक आस्थाओं की उत्पत्ति, उनका विकास तथा मानव-जीवन पर उनके प्रभाव को प्रदर्शित करना मात्र था। वही कथावाचक ने किया है। आदिमानव ने जिस रूप में आस्थाओं को ग्रहण किया, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। आदिमानव अपने विकास के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा था। इस संघर्ष में जो शक्तियाँ उसके ज्ञान की पकड़ तथा अधिकार की पहुँच से बाहर रहीं, वह उन्हें अपने विश्वासों और अपनी आस्थाओं के साथ जोड़ता गया। इन्हीं आस्थाओं और विश्वासों की नींव पर बाद में बड़े-बड़े धर्म खड़े हुए। धर्मगुरुओं तथा सूफी-संतों ने आगे चलकर आदिमानव की इस सोच की वास्तविकता का पता चलाया, उससे भ्रांतियों को अलग किया तथा जो सत्य उनके ज्ञान में आया, उसे धर्म में जोड़ दिया।
पुस्तक मानव जाति के इन्हीं पहलुओं से ही नहीं बल्कि कई अन्य पहलुओं से भी बहस करती है। यह बताती है कि मानव-समाज में पेशों के आधार पर जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई, कलाओं और शिल्पों का जन्म कैसे हुआ, साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, आदमी ने लिपि किस प्रकार सीखी, आदिमानव किस चीज पर लिखा करता था? पत्थर युग से धातु युग से आज परमाणु युग तक आदमी ने जो लंबी यात्रा की है, उसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में बहुत ही रोचक ढंग से हुआ है।
मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक किशोर अवस्था के बालकों की भ्रांतियाँ ही दूर नहीं करेगी, बल्कि परंपरागत शिक्षा के परिणामस्वरूप बने उनके चिंतन में भी गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।
मैं अपनी यह बात फिर जोर देकर कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक का सबसे बड़ा उद्देश्य आदमी की कथा को आदमी तक ही केंद्रित रखना है। उसे राजाओं, बादशाहों का बहीखाता न बनाकर तार्किक रूप से यह सिद्ध करना है कि मानव-समाज में विकास या परिवर्तन की जो मौलिक शक्तियाँ रही हैं, वे आदमी की विकसित, प्रभावित या परिवर्तित होती हुई सोच और उत्पादन के अदलते-बदलते साधनों से जुड़ी थीं। यह सही है कि आदिमानव के सामूहिक जीवन में कुछ व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक विकसित हुए तो कुछ कम, जैसे कि एक परिवार के चार बच्चों के बीच देखा जाता है। इस असमानता ने भी अधिक प्रबुद्ध और शक्तिशाली लोगों को अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों पर धाक जमाने की प्रेरणा दी होगी। बहरहाल, यह पुस्तक जिस रोचक एवं वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई है, उसके लिए लेखक निसंदेह प्रशंसा का पात्र है। इसे अधिक से अधिक हाथों में पहुँचना चाहिए, क्योंकि यह मानव-इतिहास को उसके सच्चे रूप में प्रस्तुत करती है।
चामुंडादेवी मार्ग
बिजनौर (उ.प्र.) -निश्तर ख़ानक़ाही
(1) एक उदय आदिमानव का
बड़े ही ज्ञानी आदमी थे विक्रम दा ! कंधे पर किताबों का झोला डाले भ्रमण
करते रहते। कभी यहाँ है तो कभी वहाँ। घूमना और पुस्तकें पढ़ना दो ही काम
थे विक्रम दा को। सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त कर लोग या तो बैठकर पेंशन
खाते हैं, या संन्यास ले लेते हैं, पर विक्रम दा ने ऐसा नहीं किया था। वह
अपना सारा समय अध्ययन करने या घूमने में लगाते। वे बच्चों के प्रिय थे।
लंबा कुर्ता, पायजामा, लंबी सफेद दाढ़ी। बड़ी-बड़ी प्रतिभाशाली आँखों पर
चमचमाता हुआ चश्मा। खुला-खुला माथा और लंबे बाल। ऐसे थे हमारे जगत दादा
विक्रम दा। वह बंगाली नहीं थे, फिर भी उनके नाम के साथ
‘दा’ शब्द जुड़ गया था। जैसे बच्चे अकसर मास्टर साहब
को ‘मास-साब’ और डाक्टर साहब को जल्दी में डाक
साब’ कहने लगते हैं, इसी तरह बच्चे बड़े विक्रम दादा को विक्रम
‘दा’ कहकर पुकारने लगे थे।
एक दिन घूमते-फिरते आये तो मुहल्ले के बच्चों ने घेर लिया विक्रम दा को।
‘विक्रम दा कोई अच्छी सी कहानी, विक्रम दा कोई अच्छी-सी कहानी।’
बच्चों ने जिद की तो विक्रम दा बनवारी की बैठक में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। रूमाल से ऐनक साफ करके उन्होंने दोबारा आँखों पर लगाई। बनवारी का लड़का गर्म-गर्म चाय ले आया। विक्रम दा ने चाय का घूँट लिया। मूँछों से चाय की बूँदें साफ कीं। अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से बच्चों की ओर देखा। बोले-
‘आओ बच्चो ! आज हम तुम्हें दूर अतीत की तरफ ले चलते हैं। तुम अतीत में घूमोगे तो बड़ा आनंद आएगा। तुम जान जाओगे कि आदिमानव कैसा था ? वह किस तरह रहता था ? क्या करता था ? उसने समाज की स्थापना कैसे की ? वह विकास की इस मंजिल तक कैसे पहुँचा ?’
‘पर इससे क्या लाभ होगा विक्रम दा !’ अहमद ने शरारत के साथ पूछा।
विक्रम दा ने सवाल सुना। उनकी बड़ी बड़ी आँखें फैलकर और भी बड़ी हो गईं। धीमे स्वर में बोले-
‘बच्चो ! तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि अतीत का भ्रमण करना और भविष्य के सपने देखना आदमी की दो मौलिक आदतें हैं। अगर मानव अतीत में ‘आग’ की खोज का अनुभव भुला देता तो वह बिजली के आविष्कार तक नहीं पहुँच सकता था। इसी तरह यदि वह उड़न खटोले में उड़ने का स्वप्न न देख पाता तो वह आज हवाई जहाजों में नहीं उड़ रहा होता-’
बच्चों ने विक्रम दा की बात सुनी और खुश होकर जोर जोर से तालियाँ बजाईं। विक्रम दा धीमे से मुस्कराए। फिर ऊँचे स्वर में बोले, ‘तो बच्चो, आज हम तुम्हें 20 लाख वर्ष पहले के मानव-अतीत में लेकर चलते हैं। कल्पना करो, 20-22 लाख वर्ष पहले तुम कैसे थे ? यानि आदमी कैसा था ? क्या करता था और किस तरह रहता था ?
बच्चों की आँखों में चमक आ गई। वे सब जूनियर कक्षा के छात्र थे। विक्रम दा ने अपने चारों तरफ बैठे बच्चों को देखा, ज्ञान की गंभीरता से मिलकर उनकी आवाज काफ़ी भारी हो गई थी। विक्रम दा बच्चों को लगभग 20 लाख वर्ष पुराने मानव-अतीत में लेकर चल दिए। वे बोले-
‘बच्चो ! कुछ ही वर्ष पहले पूर्वी आफ्रीका के जंगलों में कुछ खुदाइयाँ हुई हैं। वहाँ आदिमानव के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्वी अफ्रीका के बाद ऐसी खुदाइयाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी हुईं। यहाँ आदिमानव के टूटे-फूटे कंकाल तथा औजार प्राप्त हुए। इन सबसे पता चला कि धरती पर मानव का उदय कोई 18 लाख से 25 लाख वर्ष पहले हुआ था।
‘विक्रम दा ! कुछ लोग कहते हैं-तब आदमी बंदर जैसा था। बंदर से विकसित होकर ही वह आदमी बना है।’ शरद ने पूछा।
‘नहीं-नहीं,’ विक्रम दा बोले, ‘डार्विन की यह थ्योरी ग़लत सिद्ध हो चुकी है। बच्चो, आदिमानव वानर नहीं था। वह तब भी अपनी अलग पहचान रखने वाला जीव था।’
इतना कहकर विक्रम दा थोड़े रुके। फिर बोले, ‘पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणपूर्वी एशिया की खुदाइयों से आदिमानव की जो हड्डियाँ, खोपड़ियाँ मिली हैं या उसके कंकाल प्राप्त हुए हैं, उन्हें जोड़-जोड़कर पुरातनविदों ने 20 लाख वर्ष पहले के मानव के दर्शन किए थे। आओ बच्चो तुम्हें दिखाएँ कि 20-22 लाख साल पहले के युग में तुम कैसे थे ? आदिमानव कैसा था ?’
‘वह बंदर नहीं था, पर देखने में बंदर जैसा लगता था। उसका माथा आज के आदमी की तुलना में काफी छोटा था। वह हलकी सी गहराई लिए थोड़ा ढलवाँ था। आदिमानव के हाथ घुटनों के नीचे तक लटके रहते थे। उँगलियाँ काफी मोटी और कुरुप होती थीं। वह सीधा नहीं, झुककर चलता था। तुम कल्पना कर सकते हो कि चलने, पास खड़े होने में उसका आकार बिना खिंचे धनुष जैसा होता था। घुटने थोड़े-से मुड़े हुए और कमर थोड़ी-सी झुकी हुई। वह बानरों या पशुओं की तरह धरती पर चारों हाथ-पाँव टेककर नहीं चलता था। थोड़ा झुककर चलता था। अन्य जंतुओं की तुलना में वह तब भी अधिक चतुर था। फिर भी वह अधिक दक्षता से काम नहीं कर सकता था। उसके विकास का पहला चरण तब शुरू हुआ, जब उसने पत्थर से हथियार बनाने आरंभ किए।’
विक्रम दा दम लेने के लिए थोड़ा रुके। बच्चे टकटकी बाँधकर उनकी ओर देखते रहे। कुछ क्षण मौन रहकर विक्रम दा की आवाज पुनः उभरी-
‘तो बच्चो ! आदिमानव 15-15, 20-20 लोगों के समूहों में रहता था। यह उसकी विवशता थी। सुरक्षा और आहर जुटाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वह टोलियों के रूप में निकलता, धरती खोदकर वनस्पतियों की जड़ें निकालता, फल तोड़ता, जंगल से लोमड़ियाँ, खरगोश आदि जानवर पकड़ लाता। वृक्षों की खोली से पक्षियों को दबोच लेता। इन्हीं सब चीजों से वह भूख मिटाता था। खाने की जो चीजें बच रहतीं, उन्हें सुरक्षित रख लेता, ताकि वर्षा तथा प्रतिकूल मौसम में जब बाहर निकलना संभव न हो, उनसे अपना पेट भर सके। आदिमानव की गाथा सुनाते-सुनाते विक्रम दा थोड़ा रुके। एक चंचल मुस्कान उनके होठों पर आई। बोले, ‘बच्चो, तुम 20 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रहते हो। तुम अब तरह-तरह के व्यंजनों का स्वाद लेते हो। क्या तुम सोच सकते हो कि आदिमानव को अपने लिए रूखा, फीका और कच्चा भोजन जुटाना भी कितना कठिन होता था। बच्चो, तुम तो अपने-अपने घरों में सुरक्षित होकर आराम की नींद सो जाते हो। तब के मानव को हिंसक जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा करनी होती थी। अपनी रक्षा के लिए ही उसने 15-20 व्यक्तियों के समूहों में गुफाओं के अंदर रहना सीखा था। आदिमानव अधिक बड़े समूहों में इसलिए नहीं रहता था कि उसके पास बड़ी मात्रा में खाद्य-सामग्री नहीं होती थी।’
आदिमानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया बच्चो ! जब उसने पत्थर और हड्डी से हथियार बनाना तथा आग से काम लेना शुरू कर दिया।’ विक्रम दा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा-
‘बच्चो ! प्रकृति जीवन-जंतुओं को जीने की कला स्वयं सिखा देती है। आदमी के पास हिंसक जानवरों-जैसे तेज नाखूनों वाले पंजे नहीं थे। बाघ की तरह लंबे-लंबे मांसाहारी दाँत नहीं थे। वह अपने शिकार को दबोचने के लिए लंबी छलाँग भी नहीं लगा सकता था। पर बुद्धि में वह अन्य प्राणियों से चतुर था। हिंसक जंगली जानवरों के बार-बार हमलों से हताहत होने के अनुभव ने उसे अपनी सुरक्षा का मार्ग सुझाया। आदिमानव ने पहली बार पत्थर बनाना सीखा। वह पत्थरों को काट-छाँटकर मूसल-जैसे आकार के नुकीले डंडे, जमीन खोदने के धारदार भाले-जैसे उपकरण तथा फेंककर मारने वाले नोंकदार हथियार बनाने लगा था।’>br> विक्रम दा ने आदिमानव का विस्तृत परिचय देते हुए बच्चों से कहा, ‘हड्डी और पत्थरों के सीधे-सादे हथियार ही आदिमानव के विकास का पहला क्रांतिकारी अध्याय है। इनकी सहायता से वह अपने लिए बेहतर आहार प्राप्त कर सकता था तथा अपनी सुरक्षा भी अच्छे ढंग से कर सकता था। वह पत्थर की धारदार बर्छियाँ फेंककर दूसरे जंतुओं का शिकार आसानी से कर लेता था। हड्डी और पत्थर के इन हथियारों ने आदिमानव के हाथों की पहुँच को कई गुना अधिक बढ़ा दिया। उन्हें शक्ति दी और यह सोचने की क्षमता दी कि मानव अन्य जीव-जंतुओं से अधिक श्रेष्ठ है। वह हथियारों के प्रयोग से अपने लिए अधिक खाद्य-सामग्री एकत्र कर सकता है। उसे खराब मौसम तथा विपरीत परिस्थितियों के लिए बचाकर रख सकता है। हिंसक जानवरों से अपने बचाव की व्यवस्था कर सकता है। पत्थर और हड्डियों से हथियार बनाने के निरंतर परिश्रम ने उसकी उँगलियों को धीरे-धीरे अधिक लचकदार एवं सुडौल बनाना शुरू किया। शिकार के पीछे तेज-तेज भागने तथा जमीन खोदने की प्रक्रिया में मुड़ने और सीधा खड़ा होने के निरंतर प्रयास ने उसकी रीढ़ को सीधा और लोचदार बनाया। अब आदमी कमान की तरह खड़ा नहीं होता था। वह अपने घुटनों के बल पर सीधा खड़ा होना सीख गया। उसमें फुर्ती एवं चतुराई आ गई।’
यों तो आदिमानव अब भी दस-दस बीस-बीस के समूहों में छोटी-छोटी गुफाओं में ही रहता था किंतु इन प्रारंभिक हथियारों के आविष्कार ने उसे अधिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान की थी। लेकिन बच्चो, आदमी के विकास का दूसरा एवं अति महत्त्वपूर्ण चरण तब आरंभ होता है, जब उसने आग को काम में लाना और उससे अपना बचाव करना सीखा। यह कहानी मैं तुम्हें अगली भेंट में सुनाऊँगा।’
विक्रम दा ने किताबों का झोला कंधे पर डाला और अपने भ्रमण पर चल दिए।
एक दिन घूमते-फिरते आये तो मुहल्ले के बच्चों ने घेर लिया विक्रम दा को।
‘विक्रम दा कोई अच्छी सी कहानी, विक्रम दा कोई अच्छी-सी कहानी।’
बच्चों ने जिद की तो विक्रम दा बनवारी की बैठक में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। रूमाल से ऐनक साफ करके उन्होंने दोबारा आँखों पर लगाई। बनवारी का लड़का गर्म-गर्म चाय ले आया। विक्रम दा ने चाय का घूँट लिया। मूँछों से चाय की बूँदें साफ कीं। अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से बच्चों की ओर देखा। बोले-
‘आओ बच्चो ! आज हम तुम्हें दूर अतीत की तरफ ले चलते हैं। तुम अतीत में घूमोगे तो बड़ा आनंद आएगा। तुम जान जाओगे कि आदिमानव कैसा था ? वह किस तरह रहता था ? क्या करता था ? उसने समाज की स्थापना कैसे की ? वह विकास की इस मंजिल तक कैसे पहुँचा ?’
‘पर इससे क्या लाभ होगा विक्रम दा !’ अहमद ने शरारत के साथ पूछा।
विक्रम दा ने सवाल सुना। उनकी बड़ी बड़ी आँखें फैलकर और भी बड़ी हो गईं। धीमे स्वर में बोले-
‘बच्चो ! तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि अतीत का भ्रमण करना और भविष्य के सपने देखना आदमी की दो मौलिक आदतें हैं। अगर मानव अतीत में ‘आग’ की खोज का अनुभव भुला देता तो वह बिजली के आविष्कार तक नहीं पहुँच सकता था। इसी तरह यदि वह उड़न खटोले में उड़ने का स्वप्न न देख पाता तो वह आज हवाई जहाजों में नहीं उड़ रहा होता-’
बच्चों ने विक्रम दा की बात सुनी और खुश होकर जोर जोर से तालियाँ बजाईं। विक्रम दा धीमे से मुस्कराए। फिर ऊँचे स्वर में बोले, ‘तो बच्चो, आज हम तुम्हें 20 लाख वर्ष पहले के मानव-अतीत में लेकर चलते हैं। कल्पना करो, 20-22 लाख वर्ष पहले तुम कैसे थे ? यानि आदमी कैसा था ? क्या करता था और किस तरह रहता था ?
बच्चों की आँखों में चमक आ गई। वे सब जूनियर कक्षा के छात्र थे। विक्रम दा ने अपने चारों तरफ बैठे बच्चों को देखा, ज्ञान की गंभीरता से मिलकर उनकी आवाज काफ़ी भारी हो गई थी। विक्रम दा बच्चों को लगभग 20 लाख वर्ष पुराने मानव-अतीत में लेकर चल दिए। वे बोले-
‘बच्चो ! कुछ ही वर्ष पहले पूर्वी आफ्रीका के जंगलों में कुछ खुदाइयाँ हुई हैं। वहाँ आदिमानव के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्वी अफ्रीका के बाद ऐसी खुदाइयाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी हुईं। यहाँ आदिमानव के टूटे-फूटे कंकाल तथा औजार प्राप्त हुए। इन सबसे पता चला कि धरती पर मानव का उदय कोई 18 लाख से 25 लाख वर्ष पहले हुआ था।
‘विक्रम दा ! कुछ लोग कहते हैं-तब आदमी बंदर जैसा था। बंदर से विकसित होकर ही वह आदमी बना है।’ शरद ने पूछा।
‘नहीं-नहीं,’ विक्रम दा बोले, ‘डार्विन की यह थ्योरी ग़लत सिद्ध हो चुकी है। बच्चो, आदिमानव वानर नहीं था। वह तब भी अपनी अलग पहचान रखने वाला जीव था।’
इतना कहकर विक्रम दा थोड़े रुके। फिर बोले, ‘पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणपूर्वी एशिया की खुदाइयों से आदिमानव की जो हड्डियाँ, खोपड़ियाँ मिली हैं या उसके कंकाल प्राप्त हुए हैं, उन्हें जोड़-जोड़कर पुरातनविदों ने 20 लाख वर्ष पहले के मानव के दर्शन किए थे। आओ बच्चो तुम्हें दिखाएँ कि 20-22 लाख साल पहले के युग में तुम कैसे थे ? आदिमानव कैसा था ?’
‘वह बंदर नहीं था, पर देखने में बंदर जैसा लगता था। उसका माथा आज के आदमी की तुलना में काफी छोटा था। वह हलकी सी गहराई लिए थोड़ा ढलवाँ था। आदिमानव के हाथ घुटनों के नीचे तक लटके रहते थे। उँगलियाँ काफी मोटी और कुरुप होती थीं। वह सीधा नहीं, झुककर चलता था। तुम कल्पना कर सकते हो कि चलने, पास खड़े होने में उसका आकार बिना खिंचे धनुष जैसा होता था। घुटने थोड़े-से मुड़े हुए और कमर थोड़ी-सी झुकी हुई। वह बानरों या पशुओं की तरह धरती पर चारों हाथ-पाँव टेककर नहीं चलता था। थोड़ा झुककर चलता था। अन्य जंतुओं की तुलना में वह तब भी अधिक चतुर था। फिर भी वह अधिक दक्षता से काम नहीं कर सकता था। उसके विकास का पहला चरण तब शुरू हुआ, जब उसने पत्थर से हथियार बनाने आरंभ किए।’
विक्रम दा दम लेने के लिए थोड़ा रुके। बच्चे टकटकी बाँधकर उनकी ओर देखते रहे। कुछ क्षण मौन रहकर विक्रम दा की आवाज पुनः उभरी-
‘तो बच्चो ! आदिमानव 15-15, 20-20 लोगों के समूहों में रहता था। यह उसकी विवशता थी। सुरक्षा और आहर जुटाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वह टोलियों के रूप में निकलता, धरती खोदकर वनस्पतियों की जड़ें निकालता, फल तोड़ता, जंगल से लोमड़ियाँ, खरगोश आदि जानवर पकड़ लाता। वृक्षों की खोली से पक्षियों को दबोच लेता। इन्हीं सब चीजों से वह भूख मिटाता था। खाने की जो चीजें बच रहतीं, उन्हें सुरक्षित रख लेता, ताकि वर्षा तथा प्रतिकूल मौसम में जब बाहर निकलना संभव न हो, उनसे अपना पेट भर सके। आदिमानव की गाथा सुनाते-सुनाते विक्रम दा थोड़ा रुके। एक चंचल मुस्कान उनके होठों पर आई। बोले, ‘बच्चो, तुम 20 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रहते हो। तुम अब तरह-तरह के व्यंजनों का स्वाद लेते हो। क्या तुम सोच सकते हो कि आदिमानव को अपने लिए रूखा, फीका और कच्चा भोजन जुटाना भी कितना कठिन होता था। बच्चो, तुम तो अपने-अपने घरों में सुरक्षित होकर आराम की नींद सो जाते हो। तब के मानव को हिंसक जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा करनी होती थी। अपनी रक्षा के लिए ही उसने 15-20 व्यक्तियों के समूहों में गुफाओं के अंदर रहना सीखा था। आदिमानव अधिक बड़े समूहों में इसलिए नहीं रहता था कि उसके पास बड़ी मात्रा में खाद्य-सामग्री नहीं होती थी।’
आदिमानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया बच्चो ! जब उसने पत्थर और हड्डी से हथियार बनाना तथा आग से काम लेना शुरू कर दिया।’ विक्रम दा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा-
‘बच्चो ! प्रकृति जीवन-जंतुओं को जीने की कला स्वयं सिखा देती है। आदमी के पास हिंसक जानवरों-जैसे तेज नाखूनों वाले पंजे नहीं थे। बाघ की तरह लंबे-लंबे मांसाहारी दाँत नहीं थे। वह अपने शिकार को दबोचने के लिए लंबी छलाँग भी नहीं लगा सकता था। पर बुद्धि में वह अन्य प्राणियों से चतुर था। हिंसक जंगली जानवरों के बार-बार हमलों से हताहत होने के अनुभव ने उसे अपनी सुरक्षा का मार्ग सुझाया। आदिमानव ने पहली बार पत्थर बनाना सीखा। वह पत्थरों को काट-छाँटकर मूसल-जैसे आकार के नुकीले डंडे, जमीन खोदने के धारदार भाले-जैसे उपकरण तथा फेंककर मारने वाले नोंकदार हथियार बनाने लगा था।’>br> विक्रम दा ने आदिमानव का विस्तृत परिचय देते हुए बच्चों से कहा, ‘हड्डी और पत्थरों के सीधे-सादे हथियार ही आदिमानव के विकास का पहला क्रांतिकारी अध्याय है। इनकी सहायता से वह अपने लिए बेहतर आहार प्राप्त कर सकता था तथा अपनी सुरक्षा भी अच्छे ढंग से कर सकता था। वह पत्थर की धारदार बर्छियाँ फेंककर दूसरे जंतुओं का शिकार आसानी से कर लेता था। हड्डी और पत्थर के इन हथियारों ने आदिमानव के हाथों की पहुँच को कई गुना अधिक बढ़ा दिया। उन्हें शक्ति दी और यह सोचने की क्षमता दी कि मानव अन्य जीव-जंतुओं से अधिक श्रेष्ठ है। वह हथियारों के प्रयोग से अपने लिए अधिक खाद्य-सामग्री एकत्र कर सकता है। उसे खराब मौसम तथा विपरीत परिस्थितियों के लिए बचाकर रख सकता है। हिंसक जानवरों से अपने बचाव की व्यवस्था कर सकता है। पत्थर और हड्डियों से हथियार बनाने के निरंतर परिश्रम ने उसकी उँगलियों को धीरे-धीरे अधिक लचकदार एवं सुडौल बनाना शुरू किया। शिकार के पीछे तेज-तेज भागने तथा जमीन खोदने की प्रक्रिया में मुड़ने और सीधा खड़ा होने के निरंतर प्रयास ने उसकी रीढ़ को सीधा और लोचदार बनाया। अब आदमी कमान की तरह खड़ा नहीं होता था। वह अपने घुटनों के बल पर सीधा खड़ा होना सीख गया। उसमें फुर्ती एवं चतुराई आ गई।’
यों तो आदिमानव अब भी दस-दस बीस-बीस के समूहों में छोटी-छोटी गुफाओं में ही रहता था किंतु इन प्रारंभिक हथियारों के आविष्कार ने उसे अधिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान की थी। लेकिन बच्चो, आदमी के विकास का दूसरा एवं अति महत्त्वपूर्ण चरण तब आरंभ होता है, जब उसने आग को काम में लाना और उससे अपना बचाव करना सीखा। यह कहानी मैं तुम्हें अगली भेंट में सुनाऊँगा।’
विक्रम दा ने किताबों का झोला कंधे पर डाला और अपने भ्रमण पर चल दिए।
(2)
आदिमानव का आग से परिचय
विक्रम दा ने मानव समाज की स्थापना और विकास के प्रति बच्चों की दिलचस्पी
देखी तो वह नियमित रूप से उस स्थान पर आने लगे, जहाँ बैठकर उन्होंने
मान-इतिहास की यह कहानी आरंभ की थी। विक्रम दा आते तो बच्चे तालियाँ बजाकर
उनका स्वागत करते। सम्मानपूर्वक उन्हें बिठाते और ध्यानपूर्वक आदमी के
अतीत की कहानी सुनने लगते।
आज विक्रम दा आए तो आकाश पर बादल छाए थे। हलकी-हलकी वर्षा हो रही थी, हवा में ठंडक थी और नवंबर माह की सर्दी सामान्य से कुछ अधिक महसूस होने लगी थी। विक्रम दा ने कंधे पर पड़ी शाल कमर और पैरों से लपेटी और मानव-विकास की कहानी को आगे बढ़ाया-
‘बच्चो ! आदिमानव के जीवन में सबसे चमत्कारी चीज आग थी। आग से उसके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी मोड़ आया। आदिमानव आग से डरता था। जब कभी बाँस से बाँस या वक्ष से वृक्ष टकराता और वन में आग लग जाती तो आदिमानव भय से काँप उठता। तेज वर्षा में बादलों के टकराने से बिजली चमकती या उसके गिरने से आग लग जाती तो आदिमानव उसकी चमक और तपन से भयभीत हो उठता। आदिमानव आग को दैवी-प्रकोप मानता था।’
विक्रम दा यहाँ तक आकर थोड़ा रुके। उन्होंने अपने बालों की लंबी लटाओं पर हाथ फेरा। फिर बोले, ‘बच्चो, यह तो तुम जानते ही हो कि आज भी अपने मानव-समाजों में आग की पूजा की जाती है। भारत में तो आग का बड़ा धार्मिक महत्त्व है। इस परंपरा की डोर से हमें बहुत दूर अतीत में उस आदिमानव तक ले जाती है, जिसने आग को पहली बार दैविक चमत्कार के रूप में समझा और माना था।’
विक्रम दा के ललाट पर सोच की रेखाएँ उभर आई थीं। उन्होंने मानव-विकास की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा-
‘धीरे-धीरे आदमी ने आग से काम लेना सीख लिया। वह यह बात जान गया कि आग हानि पहुँचा सकती है, सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, तो आदमी को आराम भी दे सकती है। उसकी रक्षा भी कर सकती है। आदिमानव वन में लगी आग को लकड़ी आदि के माध्यम से अपनी गुफा में ले जाता। फिर बाहर लाकर उससे काम लेता। वह आग से अलाव जलाता। यह आग जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करती। ठंडे मौसम में ठंड से बचाती। गर्मी देती। आदिमानव इस आग में जमींकंद, मांस और दूसरी भोजन-सामग्री भूनकर खाने लगा। उसे लगा कि आग में भुनी हुई चीजें कच्ची वस्तुओं की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होती हैं। किंतु अभी तक वह आग को जंगल में लगने वाली आग से ही प्राप्त कर पाता था।
उसने स्वयं आग को जलाना नहीं सीखा था। इस आशंका से कि आवश्यकता पड़ने पर आग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वह अपनी गुफाओं में जलती हुई लकड़ियाँ सुरक्षित रखता। जब कभी वह किसी दूसरी जगह जाता तो जलती हुई इन लकडियों भी की साथ ले जाता, ताकि उसे आग के बिना असुविधा न हो। धीरे-धीरे आदिमानव ने यह भी सीख लिया कि आग को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। कई बार जब वह पत्थर से पत्थर को टकराता या लकड़ी को लकड़ी से बलपूर्वक रगड़ता तो उसमें से चिंगारियाँ फूटने लगतीं। इन्हीं चिंगारियों से आदिमानव ने आग जलाना सीखा। अब आग को सुरक्षित रखने के लिए उसे जलती हुई लकड़ियाँ अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं रहा। अब वह जहाँ जाता, सीखी हुई विधि से आग जला लेता। आदिमानव ने आग की विस्फोटक और लाभदायक दोनों शक्तियों को देखा था। इसलिए आग ने उसके धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान कर लिया।’
आग से आदमी के परिचय की कथा सुनाते हुए विक्रम दा ने थोड़ा दम लिया। बादल और घना हो गया था। हलकी वर्षा के साथ बार-बार बिजली कड़क जाती थी। विक्रम दा के चारों ओर बच्चे मौन धारण किए बैठे थे। वे प्रतीक्षा में थे कि विक्रम दा आदिमानव की गाथा और आगे बढ़ाएँ। बच्चों में ज्यादा जानने की उत्सुकता थी। वे जानना चाहते थे कि आज का आदमी अपने आदिकाल में कैसा था और किस प्रकार विकास करते-करते वह यहाँ तक पहुँचा ?
‘विक्रम दा ?’ मौन तोड़ते हुए शरद ने विक्रम दा से पूछा, ‘‘आदिमानव जब कमान की तरह झुककर चलता था तो उसके गाल चपटे थे और माथा चिपका हुआ था। हाथ घुटनों के नीचे झूलते रहते थे और उँगलियाँ कुरुप थीं तो फिर वह आज के आदमी की तरह सुंदर और सुडौल कैसे हो गया ?’
विक्रम दा ने शरद की बात सुनी तो गंभीर स्वर में बोले, ‘श्रम ने आदमी को बदला। मेहनत करने और गतिशील रहने के कारण आदिमानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हुए।’ इतना कहकर विक्रम दा थोड़ा रुके, फिरे बोले, ‘तुम देखते होगे बच्चो, कि मोटे पुरुष और महिलाएँ व्यायाम करके अपने-आपको सुडौल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि परिश्रम मानव-शरीर को चुस्त-दुरुस्त और फुरतीला बना देता है...।’
विक्रम दा ने श्रम के प्रभाव से आदिमानव में आए शारीरिक-मानसिक परिवर्तनों पर टिप्पटी करते हुए कहा-
‘आदिमानव ने हड्डी और पत्थर से हथियार बनाने आरंभ किए। उसने कुदाल, मूसल, चोट करने वाले हथौड़े आदि बनाए। इन्हें प्रयोग करने का तरीका सीखा। इससे उसकी सोच ही विकसित नहीं हुई, शारीरिक बनावट में भी मौलिक परिवर्तन आने लगे। हथियार बनाने और उन्हें प्रयोग करने में गतिशील रहने के कारण आदिमानव की उँगलियाँ सीधी और सुडौल हो गईं। शिकार के पीछे भागने, अपना बचाव करने या हमला करने की आवश्यकता ने उसकी रीढ़ को सीधा किया। उसमें लचक उत्पन्न की। आदिमानव की बुद्धि जैसे-जैसे विकसित हुई, उसका माथा चौड़ा और ढलवाँ होता गया। गालों के चपटेपन में उभार आया और धीरे-धीरे आदिमानव वानर की छवि से पूरी तरह अलग हो गया।
‘पत्थरों से हथियार बनाने तथा आग के आविष्कार के बावजूद आदिमानव भाषा के प्रयोग से परिचित नहीं था। वह तब इशारों और संकेतों में बात करता था।’ विक्रम दा ने आदिमानव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा-
‘बच्चो, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पंद्रह-बीस लाख वर्ष पहले के आदिमानव की आयु तब बहुत कम हुआ करती थी। वह तीस-पैंतीस वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता था। कई धर्मों में ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें बताया गया है कि आदिमानव का आकार दस-ग्यारह मीटर तक लंबा होता था। वह चार सौ-पाँच सौ वर्ष तक जीवित रहता था। किंतु शोध से यह ज्ञात हुआ है कि तब का आदमी आकार में बहुत नाटा था।
उसकी लंबाई तीन साढ़े तीन फिट होती थी और उसकी उम्र तीस-पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होती थी।’ इतना कहकर विक्रम दा ने होठों पर झुक आए अपनी मूँछों के बाल ऊपर किए और थोड़ा धीमे स्वर में बोले, ‘संभव है आदिमानव ने अपनी अल्प आयु और नाटे कद को देखकर अपने को दीर्घ आयु वाला तथा लंबे कद का मानव देखने की इच्छा की हो और इस इच्छा ने धार्मिक गाथाओं का रूप धारण कर लिया हो।’
विक्रम दा ने आदिमानव की कहानी कुछ और आगे बढ़ाई। उन्होंने बताया कि विज्ञान की परिभाषा में बीस लाख वर्ष पहले के इस आदिमानव को ‘होमो फंबर’ नाम दिया जाता है। ‘विक्रम दा ने एक बार फिर जोर देकर बच्चों को बताया-‘आदिमानव (होमो फंबर) बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस के झुंड में एक साथ गुफाओं के अंदर रहता था। महिलाएँ और पुरुष दोनों साथ-साथ आहार जुटाने के लिए परिश्रम करते थे। वह इतनी सामग्री जुटा लेते थे कि खराब मौसम तथा वर्षा आदि में आराम से बैठकर खा सकें।
‘उन दिनों का मानव जातियों में बँटा नहीं था। सब एक ही वंश के थे। संपत्ति, खाद्य-सामग्री तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएँ साझा होती थीं। हथियार बनाने और जंगली जानवरों का शिकार करने के साथ-साथ आदिमानव ने पशुओं की खाल निकालने तथा उससे अपना शरीर ढकने की कला भी सीख ली थी। खालों से बने ये वस्त्र उसे ठंड आदि से बचाते थे।’
विक्रम दा ने आदिमानव के विकास का पहला चरण बच्चों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आदिमानव साधारणतया कम ठंडे क्षेत्रों में रहा करता था। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावाद्वीप, यूरोप तथा अफ्रीका आदि देशों में आदिमानव के जो अवशेष पाए गए हैं, उनसे यही ज्ञात होता है कि किसी स्थान पर अधिक ढंड पड़ने पर यह मानव-समूह किसी अन्य क्षेत्र की ओर चले जाते थे और उन क्षेत्रों में डेरा जमा लेते थे, जहाँ उन्हें पेट भरने लायक सामग्री सुविधापूर्वक मिल सकती थी।
आदिमानव का यह समाज अब तक गोत्ररहित था। अभी विवाह-प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार का प्रचलन भी अभी नहीं हुआ। अभी तक आदिमानव किसी धर्म आदि की ओर भी नहीं आया था। वह उन प्राकृतिक चीजों के सामने नतमस्तक होता, जो उसे डरातीं या नुकसान पहुँचाती, साथ ही उन वस्तुओं को भी दैवी चमत्कार मानता, जो उसके लिए लाभदायक होती थीं। विकास के अगले चरण में आदमी ने गोत्र-व्यवस्था को अपनाया।
आज विक्रम दा आए तो आकाश पर बादल छाए थे। हलकी-हलकी वर्षा हो रही थी, हवा में ठंडक थी और नवंबर माह की सर्दी सामान्य से कुछ अधिक महसूस होने लगी थी। विक्रम दा ने कंधे पर पड़ी शाल कमर और पैरों से लपेटी और मानव-विकास की कहानी को आगे बढ़ाया-
‘बच्चो ! आदिमानव के जीवन में सबसे चमत्कारी चीज आग थी। आग से उसके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी मोड़ आया। आदिमानव आग से डरता था। जब कभी बाँस से बाँस या वक्ष से वृक्ष टकराता और वन में आग लग जाती तो आदिमानव भय से काँप उठता। तेज वर्षा में बादलों के टकराने से बिजली चमकती या उसके गिरने से आग लग जाती तो आदिमानव उसकी चमक और तपन से भयभीत हो उठता। आदिमानव आग को दैवी-प्रकोप मानता था।’
विक्रम दा यहाँ तक आकर थोड़ा रुके। उन्होंने अपने बालों की लंबी लटाओं पर हाथ फेरा। फिर बोले, ‘बच्चो, यह तो तुम जानते ही हो कि आज भी अपने मानव-समाजों में आग की पूजा की जाती है। भारत में तो आग का बड़ा धार्मिक महत्त्व है। इस परंपरा की डोर से हमें बहुत दूर अतीत में उस आदिमानव तक ले जाती है, जिसने आग को पहली बार दैविक चमत्कार के रूप में समझा और माना था।’
विक्रम दा के ललाट पर सोच की रेखाएँ उभर आई थीं। उन्होंने मानव-विकास की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा-
‘धीरे-धीरे आदमी ने आग से काम लेना सीख लिया। वह यह बात जान गया कि आग हानि पहुँचा सकती है, सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, तो आदमी को आराम भी दे सकती है। उसकी रक्षा भी कर सकती है। आदिमानव वन में लगी आग को लकड़ी आदि के माध्यम से अपनी गुफा में ले जाता। फिर बाहर लाकर उससे काम लेता। वह आग से अलाव जलाता। यह आग जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करती। ठंडे मौसम में ठंड से बचाती। गर्मी देती। आदिमानव इस आग में जमींकंद, मांस और दूसरी भोजन-सामग्री भूनकर खाने लगा। उसे लगा कि आग में भुनी हुई चीजें कच्ची वस्तुओं की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होती हैं। किंतु अभी तक वह आग को जंगल में लगने वाली आग से ही प्राप्त कर पाता था।
उसने स्वयं आग को जलाना नहीं सीखा था। इस आशंका से कि आवश्यकता पड़ने पर आग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वह अपनी गुफाओं में जलती हुई लकड़ियाँ सुरक्षित रखता। जब कभी वह किसी दूसरी जगह जाता तो जलती हुई इन लकडियों भी की साथ ले जाता, ताकि उसे आग के बिना असुविधा न हो। धीरे-धीरे आदिमानव ने यह भी सीख लिया कि आग को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। कई बार जब वह पत्थर से पत्थर को टकराता या लकड़ी को लकड़ी से बलपूर्वक रगड़ता तो उसमें से चिंगारियाँ फूटने लगतीं। इन्हीं चिंगारियों से आदिमानव ने आग जलाना सीखा। अब आग को सुरक्षित रखने के लिए उसे जलती हुई लकड़ियाँ अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं रहा। अब वह जहाँ जाता, सीखी हुई विधि से आग जला लेता। आदिमानव ने आग की विस्फोटक और लाभदायक दोनों शक्तियों को देखा था। इसलिए आग ने उसके धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान कर लिया।’
आग से आदमी के परिचय की कथा सुनाते हुए विक्रम दा ने थोड़ा दम लिया। बादल और घना हो गया था। हलकी वर्षा के साथ बार-बार बिजली कड़क जाती थी। विक्रम दा के चारों ओर बच्चे मौन धारण किए बैठे थे। वे प्रतीक्षा में थे कि विक्रम दा आदिमानव की गाथा और आगे बढ़ाएँ। बच्चों में ज्यादा जानने की उत्सुकता थी। वे जानना चाहते थे कि आज का आदमी अपने आदिकाल में कैसा था और किस प्रकार विकास करते-करते वह यहाँ तक पहुँचा ?
‘विक्रम दा ?’ मौन तोड़ते हुए शरद ने विक्रम दा से पूछा, ‘‘आदिमानव जब कमान की तरह झुककर चलता था तो उसके गाल चपटे थे और माथा चिपका हुआ था। हाथ घुटनों के नीचे झूलते रहते थे और उँगलियाँ कुरुप थीं तो फिर वह आज के आदमी की तरह सुंदर और सुडौल कैसे हो गया ?’
विक्रम दा ने शरद की बात सुनी तो गंभीर स्वर में बोले, ‘श्रम ने आदमी को बदला। मेहनत करने और गतिशील रहने के कारण आदिमानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हुए।’ इतना कहकर विक्रम दा थोड़ा रुके, फिरे बोले, ‘तुम देखते होगे बच्चो, कि मोटे पुरुष और महिलाएँ व्यायाम करके अपने-आपको सुडौल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि परिश्रम मानव-शरीर को चुस्त-दुरुस्त और फुरतीला बना देता है...।’
विक्रम दा ने श्रम के प्रभाव से आदिमानव में आए शारीरिक-मानसिक परिवर्तनों पर टिप्पटी करते हुए कहा-
‘आदिमानव ने हड्डी और पत्थर से हथियार बनाने आरंभ किए। उसने कुदाल, मूसल, चोट करने वाले हथौड़े आदि बनाए। इन्हें प्रयोग करने का तरीका सीखा। इससे उसकी सोच ही विकसित नहीं हुई, शारीरिक बनावट में भी मौलिक परिवर्तन आने लगे। हथियार बनाने और उन्हें प्रयोग करने में गतिशील रहने के कारण आदिमानव की उँगलियाँ सीधी और सुडौल हो गईं। शिकार के पीछे भागने, अपना बचाव करने या हमला करने की आवश्यकता ने उसकी रीढ़ को सीधा किया। उसमें लचक उत्पन्न की। आदिमानव की बुद्धि जैसे-जैसे विकसित हुई, उसका माथा चौड़ा और ढलवाँ होता गया। गालों के चपटेपन में उभार आया और धीरे-धीरे आदिमानव वानर की छवि से पूरी तरह अलग हो गया।
‘पत्थरों से हथियार बनाने तथा आग के आविष्कार के बावजूद आदिमानव भाषा के प्रयोग से परिचित नहीं था। वह तब इशारों और संकेतों में बात करता था।’ विक्रम दा ने आदिमानव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा-
‘बच्चो, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पंद्रह-बीस लाख वर्ष पहले के आदिमानव की आयु तब बहुत कम हुआ करती थी। वह तीस-पैंतीस वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता था। कई धर्मों में ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें बताया गया है कि आदिमानव का आकार दस-ग्यारह मीटर तक लंबा होता था। वह चार सौ-पाँच सौ वर्ष तक जीवित रहता था। किंतु शोध से यह ज्ञात हुआ है कि तब का आदमी आकार में बहुत नाटा था।
उसकी लंबाई तीन साढ़े तीन फिट होती थी और उसकी उम्र तीस-पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होती थी।’ इतना कहकर विक्रम दा ने होठों पर झुक आए अपनी मूँछों के बाल ऊपर किए और थोड़ा धीमे स्वर में बोले, ‘संभव है आदिमानव ने अपनी अल्प आयु और नाटे कद को देखकर अपने को दीर्घ आयु वाला तथा लंबे कद का मानव देखने की इच्छा की हो और इस इच्छा ने धार्मिक गाथाओं का रूप धारण कर लिया हो।’
विक्रम दा ने आदिमानव की कहानी कुछ और आगे बढ़ाई। उन्होंने बताया कि विज्ञान की परिभाषा में बीस लाख वर्ष पहले के इस आदिमानव को ‘होमो फंबर’ नाम दिया जाता है। ‘विक्रम दा ने एक बार फिर जोर देकर बच्चों को बताया-‘आदिमानव (होमो फंबर) बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस के झुंड में एक साथ गुफाओं के अंदर रहता था। महिलाएँ और पुरुष दोनों साथ-साथ आहार जुटाने के लिए परिश्रम करते थे। वह इतनी सामग्री जुटा लेते थे कि खराब मौसम तथा वर्षा आदि में आराम से बैठकर खा सकें।
‘उन दिनों का मानव जातियों में बँटा नहीं था। सब एक ही वंश के थे। संपत्ति, खाद्य-सामग्री तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएँ साझा होती थीं। हथियार बनाने और जंगली जानवरों का शिकार करने के साथ-साथ आदिमानव ने पशुओं की खाल निकालने तथा उससे अपना शरीर ढकने की कला भी सीख ली थी। खालों से बने ये वस्त्र उसे ठंड आदि से बचाते थे।’
विक्रम दा ने आदिमानव के विकास का पहला चरण बच्चों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आदिमानव साधारणतया कम ठंडे क्षेत्रों में रहा करता था। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावाद्वीप, यूरोप तथा अफ्रीका आदि देशों में आदिमानव के जो अवशेष पाए गए हैं, उनसे यही ज्ञात होता है कि किसी स्थान पर अधिक ढंड पड़ने पर यह मानव-समूह किसी अन्य क्षेत्र की ओर चले जाते थे और उन क्षेत्रों में डेरा जमा लेते थे, जहाँ उन्हें पेट भरने लायक सामग्री सुविधापूर्वक मिल सकती थी।
आदिमानव का यह समाज अब तक गोत्ररहित था। अभी विवाह-प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार का प्रचलन भी अभी नहीं हुआ। अभी तक आदिमानव किसी धर्म आदि की ओर भी नहीं आया था। वह उन प्राकृतिक चीजों के सामने नतमस्तक होता, जो उसे डरातीं या नुकसान पहुँचाती, साथ ही उन वस्तुओं को भी दैवी चमत्कार मानता, जो उसके लिए लाभदायक होती थीं। विकास के अगले चरण में आदमी ने गोत्र-व्यवस्था को अपनाया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book